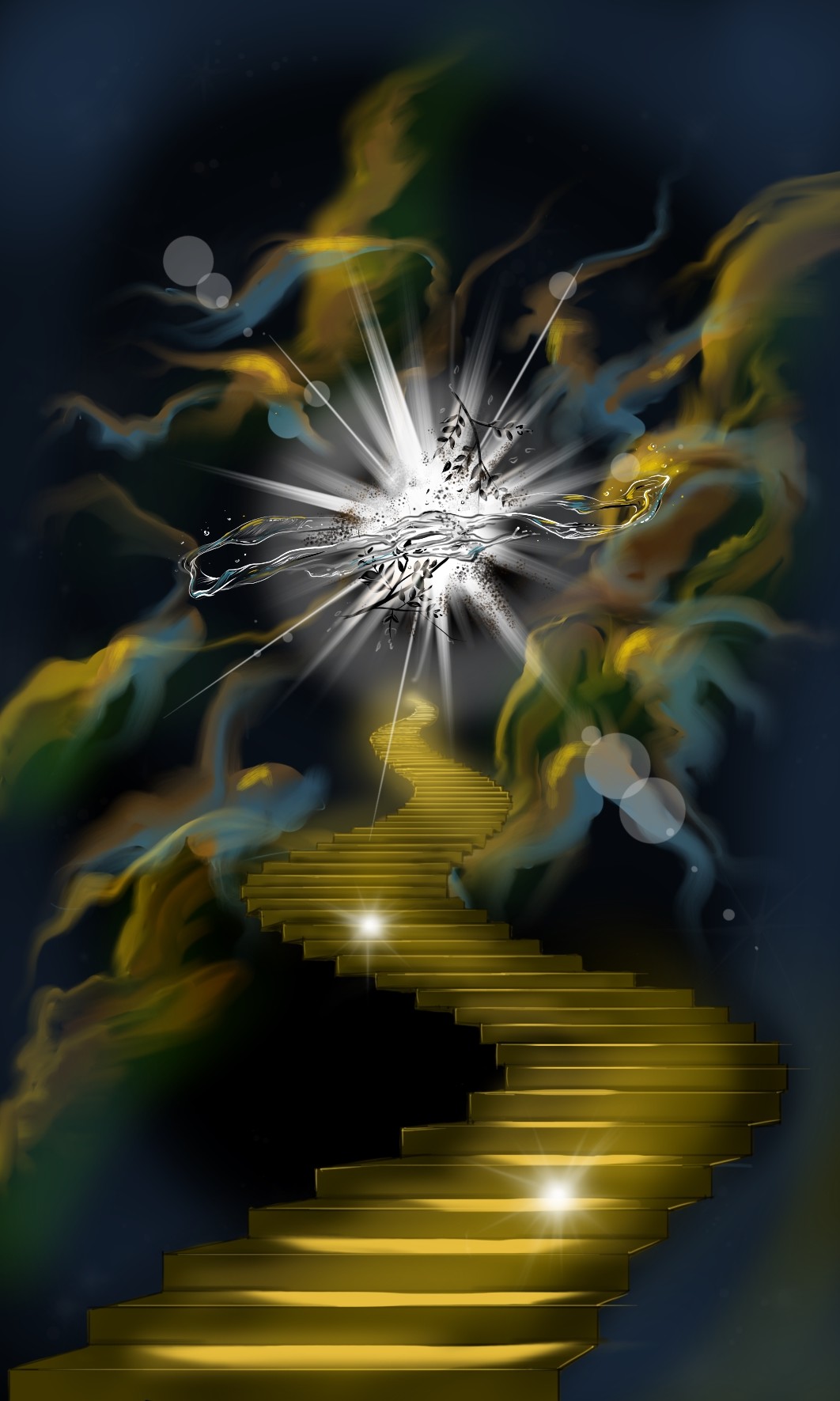'छोड़ देना' एक स्वतंत्र क्रिया नहीं है। छोड़ देने में कुछ पा लेने की क्रिया भी शामिल है। हम जब कुछ पा लेते हैं तो कुछ छोड़ देते हैं। या फिर ऐसे कह लें कि कुछ छोड़ देते हैं तो कुछ और मिल जाता है। यह 'और' कुछ भी हो सकता है। एक खालीपन भी। एक एकांत भी। एक नई दुनिया भी। एक नई मंजिल भी। कुछ भी न पाने की स्थिति नहीं होती है। मैं सोचता हूं कि माई (दादी) को ऐसा क्या मिला होगा जब उन्होंने एक मानवी की देह छोड़ी थी। क्या उनकी कल्पना के मुताबिक, उन्हें उनके अराध्य का सान्निध्य मिला होगा। या फिर उनकी ऊर्जा-चेतना को नए जड़-शरीर का निवास मिला होगा।
दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। यह भी हो सकता है कि उन्हें कुछ बेहतर मिला हो और ऐसा बेहतर मिला हो कि अपने पार्थिव शरीर को उन्होंने मुड़कर ही न देखा हो। हो सकता है कि वह यह कहते हुए तेजी से काल-पथ पर आगे बढ़ गई हों कि 'चलो, इस नरक से छुटकारा तो मिला।' यह भी हो सकता है कि उनकी चेतना कहीं और ठौर ढूंढने निकल गई हो। नए ठौर-ठिकाने को निकलने से पहले उन्होंने अपने घर को भरपूर नजर से देखा हो। अपना पूरा परिवार देखा हो, जिसे वह छोड़कर जा रही थीं।
एक-एक नातियों का नाम अपने होठों से उचारा हो। उनके चेहरे याद किए हों। भरी आंखों के धुंधले प्रकाश से अपने देवस्थान को नजर भर निहारा हो। अपने पुत्रों के माथे की शिकन देखी हो और फिर आंसू पोंछ लिए हों। दृष्टींद्रिय को छोड़कर आगे की ओर गतिमान उस गैर-शरीरी अस्तित्व को अपनी समस्त शक्ति के साथ अनिच्छा से अग्रसर किया हो।
वह याद भी कर रही हो सकती हैं, मुझे, जिसकी कोई बात उनके अवचेतन से उस दिन निकलना चाह रही थी जब मैं उनके सामने गया और वह तकरीबन बेहोशी की हालत में थीं। उनके शरीर का सोडियम बाधक हो गया। डॉक्टर ने बताया कि कम सोडियम की वजह से उनकी सेंसिबिलिटी पर बुरा असर पड़ा है। वह बातें भूल जाती हैं। मैं अब भी जानना चाहता हूं कि मेरी वह कौन सी बात थी, जो उन्हें ऐसी अवस्था में भी याद थी। उसके बाद से वह कुछ नहीं बोलीं मुझसे। मैं परेशान था। उनके ही साथ अचेत हो गया-सा। मुझे अपनी वे सारी संभावनाएं सच होती दिख रही थीं, जिन्हें लेकर मैं हमेशा भयभीत रहा करता था। हताश भी क्योंकि इतना ज्ञान तो था कि उन्हें एक दिन सच होना है।
वह सच हो गया। मेरे जीवन के सबसे बुरे माह नवंबर की 6 तारीख को। दादी का दिल बंद पड़ गया। इतना बड़ा दिल। साढ़े 8 दशक तक नेमतें बांटता रहा। आशीर्वाद देता रहा और अचानक एक दिन बंद हो गया। उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाने की तैयारी थी लेकिन वह तो ऐसा हृदय था, जिसमें कुछ भी कृत्रिम नहीं था। उसे कृत्रिम यंत्र समझते भी कैसे? कृत्रिमता ने उसे कभी स्पर्श न किया था। उस दिन कैसे कर लेता। दादी का हृदय निस्पंद हो गया। लोगों ने कहा कि वह अब नहीं रहीं।
माई चली गईं। सदैव के लिए। हमारे बीच से। हमारे घर से। हमारे गाँव से। हमारे जीवन से? नहीं जा सकतीं जीवन से। मैं उन्हें ही जी रहा हूँ। अब मैं उन्हें और ज्यादा जीने की कोशिश करूंगा क्योंकि अब वह अपने आपको नहीं जी रही हैं। अब उनके हिस्से के जीने का दायित्व भी हम पर है। हम उन्हें और ज्यादा जीने की कोशिश करेंगे।
दादी का यूं तो हमारे जीवन से जुड़े फैसलों में कोई ख़ास हस्तक्षेप नहीं था। घर के मसले भी बिना उनकी राय-मशविरे के हल हो जाते थे लेकिन इससे घर में उनकी उपयोगिता रत्ती भर भी कम नहीं थी। वह घर में एक घर के होने की जरूरत से ज्यादा जरूरी थीं। हम सभी के लिए। बेटों के लिए। बहुओं के लिए। नातियों के लिए। वह 23 लोगों के परिवार का कोई केंद्र-वेंद्र नहीं थीं और वह केवल परिधि भी नहीं थीं। वह जो थीं, उसकी ठीक-ठीक उपमा कैसे दी जाए नहीं जानता। बस ऐसे समझें कि घर के हर हिस्से में थोड़ी-थोड़ी शामिल। ऐसे गुंथी हुई कि जैसे शरीर में नसें।
यह निश्चित रूप से एक कठिन समय है क्योंकि अभी तक दादी को और घर को अलग-अलग सोचा भी नहीं गया था। अब तो इसे जीना है। जाने कब-तक। घर उपस्थित है। दादी अनुपस्थित। रिक्तता का यह झन्नाटेदार सन्नाटा सहनशीलता को भेद ही देता है। मैं दादी के देहावसान के दो दिन बाद लखनऊ भाग आया। क्योंकि यह ऐसा पूर्वज्ञात संभाव्य सत्य था, जिसकी पीड़ा से केवल भागा जा सकता था। उससे लड़ा नहीं जा सकता। यह इतना विशाल था कि हिम्मत ही नहीं हुई।
लौटना सबसे सुकूनजनक क्रिया
केदारनाथ सिंह ने लिखा- 'जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है।' इसी तर्ज़ पर कहें कि 'लौटना हिंदी की सबसे सुकूनजनक क्रिया है।' हमें लगता है कि यह है। यह उन्हें ही लग भी सकता है, जिनके पास लौटने की कोई जगह न बची हो। दादी जब तक थीं, हम कभी घर नहीं लौटे। हम दादी में लौटते थे। माई के पास। वह घर के अंदर एक घर की तरह थीं। जैसे दुनिया के अंदर लोगों का एक घर होता है, जहाँ वह लौटते हैं। मेरे लिए घर लौटना दादी के पास जाना था।
लौटना व्यापक शब्द है। इसके अर्थ में अपने आप में लौटना भी शामिल है। अपनी पूर्वचेतना को पाने का मंच। दादी घर के अंदर घर-सी थीं। उनके पास होकर हम अपने आप में लौटते थे। अवसाद, उदासी और दुःख में आगे बढ़ आए हम अपनी सामान्य चेतना में लौटते थे। इस क्रूर दुनिया में वही तो थीं, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित और स्नेहिल जगह थीं, जहाँ लौटकर नवजीवन मिलता था। किसी सुबह की तरह निर्मल, नवा और सुंदर जीवन।
प्रेम-स्नेह-मोह
प्रेम-स्नेह मोह से अलग परिस्थिति है। एक आदर्श परिस्थिति की तरह उसे देखा जाता है। उससे बाहर भी आया जा सकता है लेकिन मोह से बाहर नहीं आ सकते। मोह को इसीलिए नकारात्मकता में लिया गया। दादी की सालों की साधना इसी बात की थी कि मोह पर विजय पा ली जाए। लेकिन वह किसी दलदल की तरह इसमें धंसती गईं। पहले अपने दादाजी का मोह था। फिर पिताजी का मोह और उसके बाद दो छोटे भाइयों का। फिर इस मोह की सतह पर पुराने लोग नीचे चले गए और नए किरदार आए। इनमें उनके बेटे रहे और सबसे अंत में नाती।
दादी को अक्सर लोगों से यह कहते सुना कि उन्हें अपने बेटों से ज्यादा अब अपने नातियों का मोह होता है। यह कहते हुए हर बार उनकी आंखे भर आती थीं। इससे लगता है कि वह हर दिन जाने को तैयार थीं। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि जाना है बल्कि दुख था, कि कितने लोगों को छोड़कर जाना है। मैं अंतिम समय में उनके साथ था। मुझे तब भी उनके चेहरे पर कहीं डर नहीं दिखा। अद्भुत सहनशीलता से उन्होंने अपनी पीड़ाएं छिपा ली थीं। जिसे न हम समझ पा रहे थे, न परिवार और न ही डॉक्टर।
अचेतावस्था में भी उन्हें लगता है कि उनका भगवान अन्य प्राणियों की तरह उनसे छल कर सकता है। उनके स्मरण में, उनकी वाणी पर और उनके अंतर्मन में अपने आप को आने नहीं देगा। उन्होंने कहा, 'हमहीं के बुर्बक बूझत हवें? हम उनसे होशियार हईं।' दादी ने शायद इसी वजह से दशकों की साधना से अपने अराध्य छलिया को अपने अवचेतन में बसा रखा था। कि अंत समय में ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? चेतनाशून्य कर दोगे। अवचेतन तो फिर भी रहेगा न। उनकी साधना निष्फल नहीं थी। अपने अंतिम वक्त में उनके मुंह से जो भी उच्चरित हो रहा था, वह प्रेम-भक्ति-श्रद्धा और साधना की पराकाष्ठा से ही संभव था।
वह लगातार देव मंत्र पढ़े जा रही थीं। सुंदरकांड की चौपाइयां। गीता के गीत। भर्तृहरि की कथाएं सुनाए जा रही थीं। परीक्षित की, सुतीक्षीण की कहानियां बताए जा रही थीं। यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके पास है या नहीं? कोई उन्हें सुन रहा है या नहीं! उस वक़्त वह आदर्श कथाओं के किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ की तरह हो गई थीं। उनसे वह सब कुछ विकिरित हो रहा था जो उन्होंने जीवन भर अर्जित किया था। वह अपने ईश्वर को ही उसकी कथाएं सुनाने लगी थीं।
माई का स्वगत
माई का व्यक्तिगत जीवन बहुत उथल-पुथल भरा था। जीवन शुरू हुआ एक समृद्धि के साथ। अगाध वात्सल्य की छाया में। बाबा (दादाजी) से कहानियां सुनते। बाबूजी के स्नेह में भीगते। फिर आया संघर्षों का दौर। विवाह हो गया। एक बड़े परिवार की जिम्मेदारी के अलावा पितृसत्तात्मक समाज के दोषों के अधीन वातावरण में अपनी स्वतंत्र चेतना और अधरों के सदावसंत को बचाए रखने की जद्दोजहद ने दादी को और अधिक विनम्र और स्नेहिल बना दिया। खूब मांज दिया। वह कहतीं कि उनके दादाजी की शिक्षाएं न होतीं तो वह पता नहीं कैसे जी पातीं।
एक कहानी बताती थीं। घर में विपन्नता की स्थिति थी। परिवार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। वह उस परिवार की गाड़ी चलाने वाले की साझीदार थीं। पारिवारिक परिस्थितियां भी बहुत अनुकूल नहीं थीं। जिस प्रेम के बसंत में उन्होंने जीवन जीया था, उसके मुकाबले यह जीवन किसी त्रासदी से कम नहीं था। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति को लेकर एक सामाजिक कल्पना यही होती है कि उसके होठों से हंसी गायब हो जाए। वह दुखी रहे। मुरझाया हुआ। ऐसा नहीं था कि वह दुखी नहीं होती थीं लेकिन हंसी से पीछा नहीं छुड़ा पाती थीं। वह उनके सौंदर्य का अटूट अंग था।

एक दिन दुआर पर किसी की तलाश में टहलते वह 'सामाजिक धारणा' के विपरीत चिंतित नहीं लग रही थीं, बल्कि मुस्कुरा रही थीं। गांव के ही किसी बुजुर्ग की नजर उन पर गई थी। बाद में उसने बाबा (दादाजी) से कहा कि इतनी परेशानियों की बाद भी उन्हें कभी परेशान नहीं देखा। उनके चेहरे पर हमेशा हंसी ही देखी है। दादी को लेकर उनकी छवि ऐसे ही आनायास नहीं बन गई होगी। यह कई बार के ऑब्जर्वेशन का परिणाम था। हमने भी तो दादी को दुखी होते नहीं देखा। हमेशा हंसती-मुस्कुराती।
उस दिन भी तो वह हंस रही थीं, जब भयानक पीड़ा के बीच उन्हें गोरखपुर के फिराक चौराहे के आस्था अस्पताल में ऐडमिट कराने ले गए थे। अब उनकी हंसी याद करके रोना आ जाता है। दादी की हंसी हमारे लिए पुरस्कार जैसी थी। गाय को लाठी से नहीं मारा। अहाते से 'हट्ट-हट्ट' बोलकर भगा दिया और बाद में दादी को आकर बताया। "भला कईलऽ"। यही उनकी प्रतिक्रिया होती।
"चिड़िया खातिर पानी रखनी हईं, छत्ते पर।"
"भला कईलऽ"
"भला कईलऽ" कोई नोबल पुरस्कार जैसा था। यह सुनना भर। इन दो शब्दों ने कितने-कितने अच्छे काम हमसे कराए हैं, इस बारे में अलग से लिखा जा सकता है।
जिज्ञासु मन
सद्भावनाओं से भरे ह्रदय के अलावा उनके पास ऐसा जिज्ञासु मन था कि अंत समय तक वह विद्यार्थिनी रहीं। उन्हें आप कभी भी कुछ नया सिखाएं, वह किसी शिष्या की भांति बड़े ध्यान से सुनने बैठ जातीं। विज्ञान के रहस्यों पर भी उन्हें भरोसा हो जाता और ईश्वर पर तो खैर, विश्वास ही नहीं था, वह उसे ऐसे ट्रीट करतीं जैसे वह उनका कोई पड़ोसी या रिश्तेदार हो, जिससे उनका रोज का हाल-चाल वाला व्यवहार हो। उनके पिता ने उन्हें स्कूल कभी नहीं भेजा। दादाजी ने सिफारिश की। बहुत तेज दिमाग है स्कूल भेजो लेकिन शांति (दादी) कभी स्कूल नहीं गईं। अपने तेज दिमाग से शांति ने सद्भावना सीखी। दया करना सीखा। प्रेम लुटाना सीखा। करुणा सीखी। दूसरों की तकलीफ स्वयं में धारण करना सीखा।
स्वगत से विश्वगत
स्वार्थ मानवीय गुणों का ऐसा तत्व है, जिससे आप इससे हथियार भी बना सकते हैं और घर भी बना सकते हैं। दादी का स्वार्थ बड़े परिसर में था। वह संकुचित नहीं था। वह फैलता था, जिसमें सारा संसार समाहित हो सकता था। एक कहानी बताती थीं। किसी तीर्थयात्रा से लौट रही थीं। ट्रेन में बैठी थीं। किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो एक विद्यार्थी लड़का हांफते हुए डिब्बे में चढ़ गया और जगह ढूंढने लगा। जहाँ भी शरण मांगता, लोग भगा देते। माई यह दृश्य देख रही थीं। बोलीं, "आवऽ, बच्चा। हमरे लग्गे आवऽ। हम देब तुहके जगहि। अइसहीं हमरो नातिया कुल आवत होइहें नऽ, हाँफ़त-परेशान होत। तुहूँ हमारे नतिये खान बाटऽ।" (मेरे पास आओ। हम जगह देंगे। ऐसे ही हमारे पोते भी आते होंगे। तुम भी मेरे नाती जैसे ही हो।) मैं जब भी इस कहानी का दृश्य बनाता हूँ, रो पड़ता हूँ और माई के प्रति कृतज्ञता के एक सागर में गिर पड़ता हूँ।


अजीवन समझदार बच्ची
दादी जीवन भर एक समझदार बच्ची रहीं। उत्सुकता से सबकी बात सुनतीं। जो भी पढ़तीं, उसे सुनाने के लिए बेचैन हो जातीं। जैसे जब हम छोटे थे तब स्कूल में क्या हुआ, रास्ते में क्या देखा, सब मम्मी को बताने के लिए बेचैन हो जाते थे। दादी के भाई का कुछ ही साल पहले कैंसर से निधन हो गया था। वह उन्हें अक्सर बुला लेते थे। अध्ययनशील व्यक्ति थे। बहुत पढ़ते थे। पढ़ा हुआ किसी को समझाना होता था तो वह अपनी दीदी को बुला लेते। दादी उन्हें बड़ी गंभीरता से सुनतीं। याद भी रखती थीं और जब घर लौटतीं तब हमें सुनाती थीं। कुछ तथ्य भूलते तब अपनी याददाश्त को कोसतीं। दूसरे ही पल उन्हें याद हो आता। राजनीतिक बहसें भी दिलचस्पी से सुनतीं। उन्हें किसी भी चीज के बारे में सूचना दी जा सकती थी। इतनी अबोध और अहंकारशून्य की किसी से भी ज्ञान लेने में संकोच नहीं था।
घर के सबसे छोटे बच्चे से लेकर गुरु परिवार के विद्वान लोगों तक के बताई चीजों को ध्यान से सुनतीं। राजनीति पर बात चलती तो पल भर में नरेंद्र मोदी का समर्थन होता और थोड़ी देर में ही उनके खिलाफ हो जातीं। यह निर्भर करता कि कौन उन्हें नरेंद्र मोदी के कामों के बारे में जानकारी दे रहा है। नातियों पर ऐसा भरोसा कि किसी पर भी अविश्वास नहीं करती थीं। मुझे लगता है कि वह ऐसा इसलिए करती थीं कि उन्हें हमें किसी भी तरह से निराश नहीं करना होता था। इसलिए, सबकी बात सही। सब पर प्रतिक्रिया। सबके हिसाब से खुश हो लेना। सबकी हंसी में हंस देना।
अंतिम दिन
वह अंतिम दिन था घर पर उनका। अपने घर पर, जिसके लिए वह कहतीं कि अब यहीं से जाना है। हम उस 'जाना' का अर्थ समझते थे। हम जानते थे कि यह 'जाना' जिस दिन होगा, हम रोक नहीं पाएंगे। वैसे ही जैसे उन्हें रुद्रपुर में नहीं रोक पाते थे। एक दिन भी अतिरिक्त। वह दुग्धेश्वरनाथ मंदिर में पूजा करने गांव से आ जाती थीं। हम लोगों में जैसे उत्साह का नवसंचार हो जाता। एक मुरझाया हुआ जीवन खिल जाता। वह दो-तीन दिन रहतीं, फिर जाने को कहतीं।
बिल्कुल भी जी नहीं चाहता कि उन्हें जाने दें लेकिन वह बेहद करुणा के साथ कहतीं कि उन्हें अब घर जाना है। फिर लगता कि दादी को उनके घर से अलग करना कितनी बड़ी क्रूरता है। वह यहां अपने आपको अडजस्ट नहीं कर पाती थीं। अतिथि की तरह रहती थीं। हम अपनी माई को अपने घर में अतिथि के रूप में कभी नहीं देख सकते थे। इसलिए, अपना आग्रह छोड़ देते और वादा करते कि जल्दी ही छुट्टियों में घर आएंगे।
वह अंतिम दिन था। जब हम घर पहुंचे तो चाची, मां और बुआ उन्हें घेरकर बैठी थीं। दादी लगातार बोले जा रही थीं। कुछ न कुछ सुना रही थीं। जितने संस्कृत श्लोक उन्हें याद थे, सब बारी-बारी से बांचे जा रही थीं। दादी जिंदगी भर अस्पताल नहीं गईं। वह तब भी नहीं जाना चाहती थीं लेकिन हमलोग अचेतन अवस्था में उन्हें वहां से गोरखपुर ले गए। जीवनभर इस पर मन में द्वंद्व रहेगा कि कहीं अस्पताल ले जाकर गलती तो नहीं की गई कि उनकी उस अभिलाषा को भी पूरा नहीं होने दिया, जिसमें वह यहीं से 'जाना' चाहती थीं। लेकिन दादी को उस असहाय अवस्था में देख भी तो नहीं सकते थे। अत्यंत स्वावलंबी, अत्यंत सशक्त और अत्यंत आत्मनिर्भरता की अवस्था में ही हमेशा उन्हें देखा गया था। ऐसी हालत में अपार कष्ट झेलते भी तो नहीं देख सकते।


आराम करना तो उनकी फितरत में था नहीं और वह पूरे दिन बिस्तर पर रहीं। बार-बार उठना भी तो चाह रही थीं। बार-बार हाथ आगे बढ़ाकर सहारा मांगती। हम रोक देते। "माई अब्बे नाईं। बोतल चढ़त बा।" दादी बोलतीं- "अच्छा, अब्बे नाईं?" फिर स्वीकार्यता का संकेत देकर लेट जातीं। यह क्रिया कई बार दोहरातीं। जिद नहीं थी। चिड़चिड़ापन नहीं था। इतना नियंत्रण कैसे था, मुझे नहीं पता। फिर कोई किसी पुराण कथा के बारे में पूछ देता तो तफसील से बताने लग जातीं। ऐसा जीवंत था उस कर्मठी और चिर युवती महिला का अपने घर पर अंतिम दिन।
हालांकि, घर पर अंतिम दिन और संसार में सदेह अंतिम दिन, दोनों घटनाएं एक ही दिन नहीं घटीं। अपने उपन्यास 'अपने-अपने अजनबी' में अज्ञेय लिखते हैं न कि "कुछ भी किसी के बस में नहीं है। एक ही बात हमारे बस की है, और वह है इस बात को पहचान लेना।" इस बात को पहचान लेना चाहिए। दादी का अंतिम क्षण आया कार्तिक की नवमी को। उसे अक्षय नवमी का दिन कहा जाता है। दादी स्वस्थ होतीं तो दिया जलाने के लिए दुग्धेश्वर नाथ मंदिर जातीं लेकिन इस बार उन्हें एक दीया बुझाना था। 'अक्षय' शब्द की संगत वाले दिन को इस शब्द के विरुद्ध जाना था और यह 'जाना' अपने घर नहीं हुआ, जैसाकि वह चाहती थीं।
स्मृतियों तक की यात्रा
"कौन स्वतंत्र है? कौन चुन सकता है कि वह कैसे रहेगा या नहीं रहेगा?" कोई नहीं न! दादी भी इसका अपवाद नहीं बन सकीं। जीवन से स्मृति में स्थापित हो गईं। हमें अंत तक उम्मीद थी कि दादी लौटेंगी। आज तक हम उनमें लौटते थे। आज वह हममें लौटेंगी। लेकिन इस बार लौटना नहीं हुआ। इस बार 'जाना' तय हुआ। स्मृतियों में। हमारी स्मृतियों में। घर की स्मृतियों में। घर की फुलवारी की स्मृतियों में। घर के अहाते की स्मृतियों में। घर के आंगन, छत के देवस्थान की स्मृतियों में। हम याद करेंगे उन्हें हमेशा क्योंकि गीत चतुर्वेदी कहते हैं कि "हम जब तक किसी को याद करते हैं उसकी मृत्यु नहीं होती।"